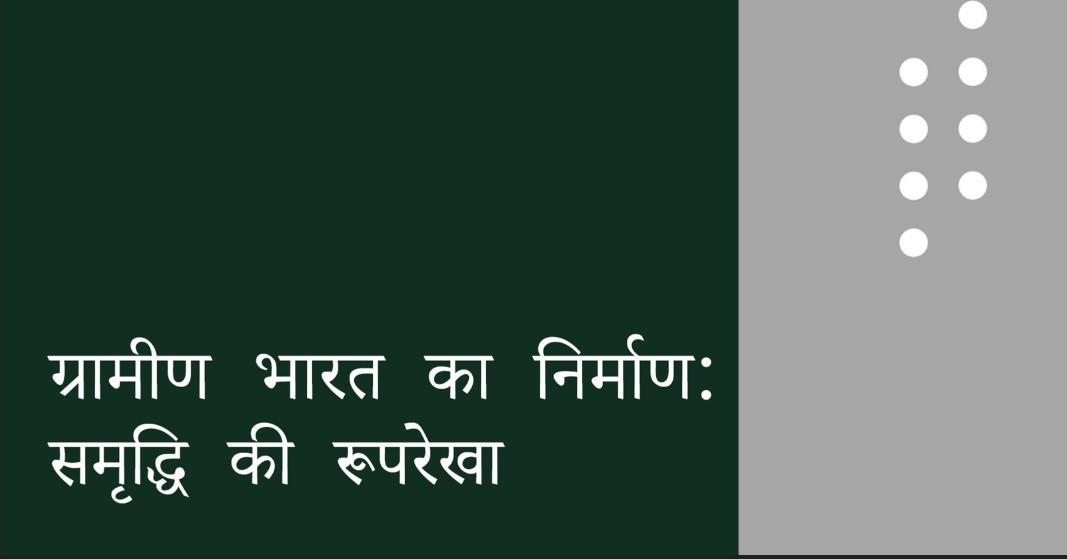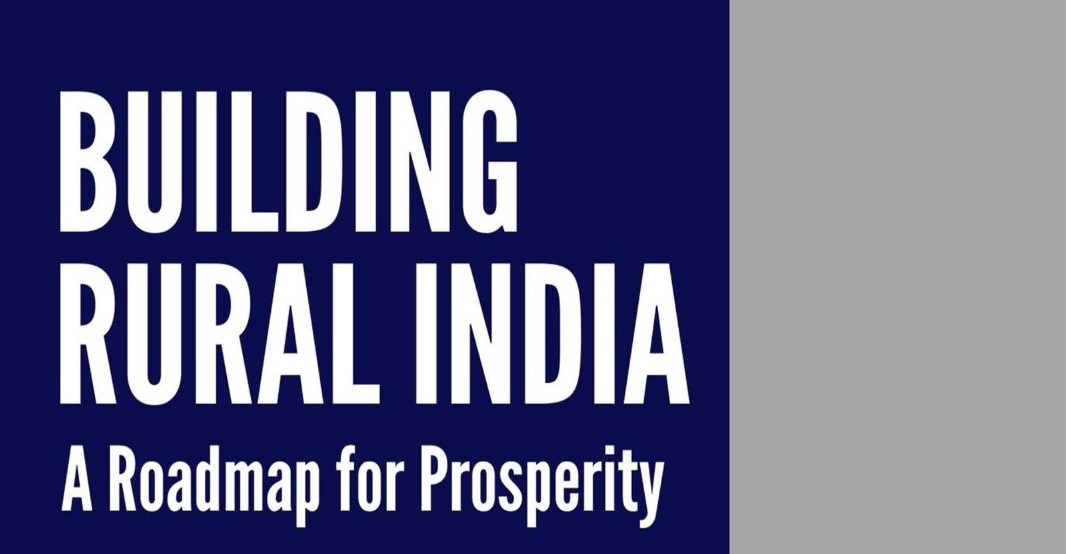स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना: उपयोगिता, लचीलापन और सततता के लिए डिज़ाइन करना
सारांश
तेज़ ग्रामीण परिवर्तन, न्यायसंगत और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारत जैसे देशों में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र लगभग 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह शोध पत्र उपयोगिता, लचीलापन और सततता के सिद्धांतों को समाहित करते हुए स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना के विकास की अनिवार्यता की जाँच करता है। इसमें यूरोपीय संघ की स्मार्ट विलेज पहल, चीन की डिजिटल विलेज रणनीति तथा उप-सहारा अफ्रीका में विकेंद्रीकृत ऑफ-ग्रिड प्रणालियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आधार बनाकर भारत की नीतिगत परिदृश्य का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और भारतनेट जैसी प्रमुख प्रमुख योजनाओं को रेखांकित किया गया है। विश्लेषण में प्रमुख नीतिगत खामियों की पहचान की गई है, जिनमें विखंडित योजना, संचालन और रखरखाव हेतु अपर्याप्त वित्तपोषण, सीमित जलवायु अनुकूलन उपाय और निरंतर बना हुआ डिजिटल अंतर शामिल हैं। इसके समाधान के लिए यह शोध पत्र एक एकीकृत ढाँचे का प्रस्ताव करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभिसरण, समुदाय-आधारित शासन, जलवायु-लचीले डिज़ाइन मानक तथा जमीनी स्तर पर डिजिटल क्षमता के सुदृढ़ीकरण पर बल देता है।
वैश्विक अनुभवों और भारत की विकसित होती संस्थागत परिस्थितियों के समन्वय द्वारा यह अध्ययन ग्रामीण अवसंरचना को समावेशी विकास और जलवायु लचीलापन का प्रेरक मानते हुए सतत विकास लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुरूप विमर्श को आगे बढ़ाता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, विकास कार्यकर्ताओं और ग्रामीण परिवर्तन से जुड़े स्थानीय शासन संस्थानों के लिए ठोस कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
कीवर्ड्स: स्मार्ट गाँव, ग्रामीण अवसंरचना, जलवायु लचीलापन, सतत विकास, भारत
परिचय
वैश्विक स्तर पर, स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जो शहरी–ग्रामीण विकास के बीच बढ़ती खाई को पाटने का एक व्यावहारिक साधन है। यह शब्द एकीकृत भौतिक और डिजिटल अवसंरचना प्रणालियों को संदर्भित करता है, जो जलापूर्ति, सड़कें, ऊर्जा, स्वच्छता, आवास और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सेवाओं की कुशल आपूर्ति को सक्षम बनाते हैं, साथ ही जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन और दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करते हैं (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन [OECD], 2020)। संयुक्त राष्ट्र (2021) के अनुसार, विश्व की 43% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इन समुदायों को अक्सर जीवनयापन, स्वास्थ्य और शिक्षा को समर्थन देने वाली अवसंरचना तक समान पहुँच नहीं मिलती।
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण दर्शाते हैं कि जब ग्रामीण अवसंरचना को स्मार्ट ढंग से डिज़ाइन किया जाता है, तो यह न केवल उपयोगिता में सुधार करती है बल्कि समुदायों को पर्यावरणीय और आर्थिक झटकों का सामना करने में भी सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की स्मार्ट विलेज पहल ग्रामीण बस्तियों में डिजिटल और सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देती है ताकि जनसंख्या में कमी, आर्थिक ठहराव और सेवा अंतराल का समाधान किया जा सके (ENRD, 2018)। इसी प्रकार, चीन के ग्रामीण स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश ने गरीबी उन्मूलन के उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं (Zhou et al., 2020)। हालांकि, अब भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि किफ़ायती दरें सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रणालियों की पारस्परिक संगतता और इन प्रणालियों का सामुदायिक स्वामित्व (Li et al., 2022)।
भारत में दांव और भी बड़े हैं। भारत की लगभग 65% आबादी, यानी लगभग 90 करोड़ लोग, अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)। हालाँकि ग्रामीण सड़कों (पीएमजीएसवाई के तहत 2000 से अब तक 7,00,000 किमी से अधिक सड़कें बनाई गईं) और विद्युतीकरण (2019 तक लगभग 100% गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता, रखरखाव और जलवायु लचीलापन अब भी चुनौतियाँ बने हुए हैं (एशियन डेवलपमेंट बैंक, 2022; नीति आयोग, 2021)। भारत अवसंरचना रिपोर्ट (IDFC Institute, 2022) के अनुसार, लगभग 55% ग्रामीण परिवारों के पास पाइप जल आपूर्ति की विश्वसनीय पहुँच नहीं है और 50% से अधिक परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है।
इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन अवसंरचना की कमजोरियों को और बढ़ाता है। विश्व बैंक (2021) का अनुमान है कि यदि अनुकूलनशील अवसंरचना प्रणालियों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो 2030 तक जलवायु परिवर्तन 4.5 करोड़ से अधिक दक्षिण एशियाई लोगों को गरीबी में धकेल सकता है। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) बढ़ते हुए ग्रामीण सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और आवास में सततता और लचीलापन शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी तरह, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकेंद्रीकरण और सामुदायिक-आधारित मॉडलों पर बल देते हैं ताकि सततता सुनिश्चित हो सके (MoJS, 2022)।
नीतिगत विमर्श एक नवोन्मेषी स्मार्ट विलेज फ्रेमवर्क की ओर विकसित हो रहा है, जिसमें डिजिटल उपकरण, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और जलवायु-लचीली निर्माण तकनीकें शामिल हैं (Kumar et al., 2021)। फिर भी, इस दृष्टि को लागू करने के लिए विभिन्न योजनाओं का अभिसरण, स्थानीय सरकारों की क्षमता निर्माण और वित्त तक पहुँच आवश्यक है।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) विशेषकर एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) और एसडीजी 11 (सतत शहर और समुदाय) के अनुरूप होने के लिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण अवसंरचना केवल मात्रात्मक रूप से विस्तारित न हो, बल्कि उसे दीर्घकालिक उपयोगिता, लचीलापन और सततता के लिए डिज़ाइन किया जाए (संयुक्त राष्ट्र, 2021)। जैसे-जैसे भारत अपने अमृत काल (2047) की दृष्टि की ओर बढ़ रहा है, स्मार्ट, समावेशी और जलवायु-अनुकूल ग्रामीण अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना न्यायसंगत विकास हासिल करने के लिए निर्णायक होगा।
यह शोध पत्र इस बात की जाँच करता है कि भारत किस प्रकार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय नवाचारों का उपयोग करके अपनी ग्रामीण अवसंरचना रूपरेखा को सुदृढ़ कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक ढाँचे में भारत की पहलों का संदर्भ देकर यह नीति-निर्माताओं, विकास कार्यकर्ताओं और स्थानीय शासन संस्थानों को स्मार्ट, समावेशी और जलवायु-लचीली ग्रामीण अवसंरचना प्रणालियों को पैमाने पर लागू करने के मार्ग सुझाता है। यह अध्ययन भारत की ग्रामीण अवसंरचना की दिशा को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थापित करता है और यूरोपीय संघ की स्मार्ट विलेज रूपरेखा, चीन की डिजिटल विलेज रणनीति तथा उप-सहारा अफ्रीका में विकेंद्रीकृत ऑफ-ग्रिड मॉडलों से अनुभवजन्य सबक लेता है। इसके बाद यह भारत के प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों जैसे ग्रामीण सड़कें, सुरक्षित पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी और जलवायु अनुकूलन की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन की खामियों और नीतिगत चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस समन्वय के आधार पर यह उपयोगिता-प्रेरित, जलवायु-लचीली और सामाजिक रूप से सतत प्रणालियों के डिज़ाइन और क्रियान्वयन हेतु साक्ष्य-आधारित सिफ़ारिशें प्रदान करता है। इसका प्रमुख योगदान अंतर्राष्ट्रीय अंतर्दृष्टियों और भारत के विकसित हो रहे संस्थागत ढाँचों के बीच सेतु बनाने में है, जिससे रूपांतरणकारी और न्यायसंगत ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत रोडमैप उपलब्ध हो सके।
प्रमुख योजनाएँ और स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना: भारत की सामरिक दृष्टि
भारत में ग्रामीण अवसंरचना विकास स्वतंत्रता के बाद से ही एक केंद्रीय नीतिगत प्राथमिकता रहा है, जहाँ विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। देश का सामरिक प्रयास अपने ग्रामीण परिदृश्य को बदलने पर केंद्रित है, जिसमें अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, विश्वसनीय बुनियादी सेवाएँ और सतत आर्थिक विकास की आधारशिला प्रदान करना शामिल है। पहले की तरह खंडित हस्तक्षेपों के विपरीत, समकालीन दृष्टिकोण पारंपरिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्मार्ट तकनीकों, समुदाय-आधारित शासन और जलवायु-लचीले डिज़ाइनों के साथ एकीकृत करता है।
ग्रामीण सड़कें और कनेक्टिविटी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), जिसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, ने भारत की 97% से अधिक पात्र बस्तियों को सभी मौसमों में उपयोगी सड़कों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)। मार्च 2023 तक 7,24,000 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण गतिशीलता, खेत से बाज़ार तक की कड़ी, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (नीति आयोग, 2021)।
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के अंतर्गत सड़क अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनी हुई है, जहाँ ग्रामीण सड़कों को एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ निरंतर आवंटन मिल रहा है। वित्त मंत्रालय (2023) के अनुसार, सड़क अवसंरचना के लिए NIP के तहत FY2025 तक लगभग ₹20 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें सार्वभौमिक ग्रामीण कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता के कारण ग्रामीण सड़कों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। PMGSY-III विशेष रूप से जलवायु-लचीली सड़कों पर बल देता है, जिसमें बिटुमेन के लिए कोल्ड मिक्स तकनीक और भू-स्थानिक निगरानी प्रणालियों जैसी तकनीकों का समावेश किया जा रहा है ताकि सड़कों की टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)।
सुरक्षित और सतत पेयजल: जल जीवन मिशन
भारत की ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना ऐतिहासिक रूप से बिखरी हुई रही है और गहरे बोरवेल पर निर्भर रही है, जिसके परिणामस्वरूप असतत दोहन और खराब सेवा गुणवत्ता सामने आई। जल जीवन मिशन (JJM), जिसे 2019 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है। जल शक्ति मंत्रालय (2023) के अनुसार, मार्च 2024 तक लगभग 62% ग्रामीण परिवार (लगभग 12.3 करोड़) जल जीवन मिशन के अंतर्गत कवर किए जा चुके थे, जो 2019 के मात्र 17% से एक उल्लेखनीय छलांग है।
केंद्रीय बजट 2024–25 में जल जीवन मिशन के लिए ₹70,000 करोड़ आवंटित किए गए, जो ग्रामीण कल्याण और महिला सशक्तिकरण में इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2024)। यह कार्यक्रम स्रोत सततता, ग्रे-वाटर प्रबंधन और गाँव स्तर पर ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (O&M) मॉडलों पर विशेष जोर देता है, जो लचीली और सतत जल अवसंरचना की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है (जल शक्ति मंत्रालय, 2023)।
डिजिटल अवसंरचना: भारतनेट और आगे
डिजिटल कनेक्टिविटी को व्यापक रूप से स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना की आधारशिला माना जाता है। भारतनेट परियोजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहलों में से एक है, का उद्देश्य 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ना है (दूरसंचार विभाग, 2023)। वर्ष 2024 की शुरुआत तक लगभग 2,00,000 गाँवों में फाइबर बिछाया जा चुका था और 1,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतें सेवा-तैयार थीं (TRAI, 2024)।
केंद्रीय बजट 2024–25 में डिजिटल अवसंरचना की रीढ़ को मजबूत करने हेतु लगभग ₹14,000 करोड़ आवंटित किए गए, साथ ही दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतनेट का एकीकरण कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और डिजिटल इंडिया ढाँचे के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता पहलों के साथ मिलकर गाँवों में ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, डिजिटल भुगतान और स्मार्ट गवर्नेंस को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है (DoT, 2023)।
इन प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे अंतिम छोर तक वाई-फाई पहुँच, संचालन एवं रखरखाव (O&M) के लिए स्थानीय उद्यमिता, और वंचित वर्गों में डिजिटल साक्षरता (Mehta et al., 2023)। इन खाइयों को तेजी से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और स्थानीय सहकारी मॉडलों के माध्यम से दूर किया जा रहा है।
कोल्ड चेन और कृषि-लॉजिस्टिक्स: उपयोगिता और सततता के लिए महत्वपूर्ण
कृषि भारत की 50% से अधिक ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत बनी हुई है, फिर भी अपर्याप्त भंडारण और कोल्ड चेन अवसंरचना के कारण होने वाले फसल कटाई पश्चात नुकसान का अनुमान प्रतिवर्ष ₹92,000 करोड़ है (ICRIER, 2021)। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में कृषि-लॉजिस्टिक्स, एकीकृत कोल्ड चेन और आधुनिक पैकहाउस सहित बड़े पैमाने पर वित्तीय आवंटन किया गया है।
केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और कृषि-इंफ्रा फंड के विस्तार की घोषणा की गई, जिसके तहत ग्रामीण कोल्ड चेन और मूल्य-वर्धित सुविधाओं के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, 2024)। स्मार्ट कोल्ड चेन, जो तापमान और खराबी नियंत्रण के लिए IoT-आधारित निगरानी का उपयोग करती हैं, किसानों की आय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती हैं और खाद्य अपव्यय को कम कर सकती हैं, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है (कुमार और सिंह, 2022)।
उभरते स्मार्ट गाँव मॉडल: एकीकृत और समुदाय-प्रेरित
क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं से आगे बढ़ते हुए, भारत का नीतिगत विमर्श तेजी से एकीकृत स्मार्ट गाँव मॉडलों की ओर बढ़ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने ऐसे स्मार्ट गाँव पायलट किए हैं, जो सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सोलर माइक्रो-ग्रिड, डिजिटल सेवाएँ और जलवायु-लचीले आवास में निवेश को एकीकृत करते हैं (शर्मा और कुमार, 2022)। ये पहलें यूरोपीय संघ की स्मार्ट विलेज अवधारणा जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेती हैं, लेकिन इन्हें स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार अनुकूलित किया गया है।
स्मार्ट गाँव दृष्टिकोण सामान्यतः निम्नलिखित पर बल देता है:
• ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत योजना।
• समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व।
• सेवा आपूर्ति और शासन के लिए डिजिटल उपकरण।
• विकेंद्रीकृत आपूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ।
• जलवायु परिवर्तनशीलता के अनुकूलन के लिए लचीला आवास और वॉश (WASH) अवसंरचना।
उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की स्मार्ट गाँव पहल वाई-फाई कनेक्टिविटी, डिजिटल कक्षाएँ, टेलीमेडिसिन और सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटिंग को एक साथ जोड़ती है (स्मार्टगाँव फाउंडेशन, 2023)। इसी बीच, भारत सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत मॉडल गाँव पर आधारित पायलट परियोजना एक ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करती है, जो स्पष्ट सततता मानकों के साथ एकीकृत और स्मार्ट हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर लागू करने का मार्ग दिखाती है (नीति आयोग, 2023)।
अभिसरण और लचीले नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र की ओर
नीतिगत परिदृश्य अब अभिसरण और जीवनचक्र योजना की ओर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जल जीवन मिशन, भारतनेट और पीएमजीएसवाई को बढ़ते हुए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के माध्यम से पंचायत राज मंत्रालय के तहत एकीकृत किया जा रहा है। यह निवेशों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में मदद करता है और साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करता है (पंचायती राज मंत्रालय, 2023)।
हालाँकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल हार्डवेयर निवेश पर्याप्त नहीं हैं, यदि इनके साथ मजबूत ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) प्रणालियाँ, सामुदायिक क्षमता निर्माण और जलवायु अनुकूलन उपाय नहीं जोड़े जाते (विश्व बैंक, 2021)। उदाहरण के लिए, पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई ग्रामीण सड़कों में अब जलवायु जोखिम मूल्यांकन और लचीले डिज़ाइन तत्वों को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में ऊँचे तटबंध और बेहतर जल निकासी प्रणाली (एडीबी, 2022)।
वैश्विक अध्ययन: क्रियान्वयन में स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना
यूरोपीय संघ की स्मार्ट विलेज पहल
वैश्विक स्तर पर सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक यूरोपीय संघ (EU) की स्मार्ट विलेज अवधारणा है, जो कई सदस्य देशों में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट और सेवाओं के ह्रास के प्रत्युत्तर के रूप में उभरी। स्मार्ट विलेज के लिए ईयू एक्शन प्लान उन्हें ऐसी समुदायों के रूप में परिभाषित करता है जो डिजिटल और सामाजिक दोनों प्रकार के नवाचारपूर्ण समाधानों का उपयोग करके अपनी लचीलापन, सेवा आपूर्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं (ENRD, 2018)।
उदाहरण के लिए, फ़िनलैंड के कंगासनिएमी गाँव ने ग्रामीण युवाओं के पलायन और सीमित स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती से निपटने के लिए एक डिजिटल को-वर्किंग हब और ई-हेल्थ टेलीमेडिसिन सेवाएँ विकसित कीं (OECD, 2020)। इसी तरह, फ्रांसीसी आल्प्स के लेस ऑरेस गाँव ने स्मार्ट ऊर्जा ग्रिड, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और स्मार्ट नवाचारी पर्यटन समाधान अपनाए, जिन्होंने न केवल ऊर्जा लागत को कम किया बल्कि स्थानीय रोज़गार में भी वृद्धि की (Dax et al., 2019)।
यूरोपीय ग्रामीण विकास नेटवर्क (ENRD, 2018) के अनुसार, 40 से अधिक पायलट स्मार्ट विलेज परियोजनाओं ने यह प्रदर्शित किया है कि जब ग्रामीण समुदायों को डिजिटल उपकरणों, शासन क्षमता और स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से सशक्त किया जाता है, तो वे निवेश आकर्षित कर सकते हैं, युवाओं को गाँव में रोक सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित कर सकते हैं। ईयू की कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी (CAP) और लीडर कार्यक्रम इन दृष्टिकोणों को विस्तार देने के लिए समर्पित वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं।
चीन: डिजिटल विलेज और ग्रामीण स्मार्ट ग्रिड
चीन की डिजिटल विलेज रणनीति (2021–2025) एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। पिछले एक दशक में, चीन ने स्मार्ट ग्रिड, ग्रामीण ब्रॉडबैंड और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी है, जिससे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है (Li et al., 2022)। ताओबाओ विलेज मॉडल इसका एक प्रमुख उदाहरण है: ये ऐसे ग्रामीण क्लस्टर हैं जहाँ ई-कॉमर्स की पहुँच स्थानीय परिवारों के 10% से अधिक तक है, जिससे किसान और कारीगर सीधे अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहरी बाज़ारों में बेच सकते हैं (Zhou et al., 2020)।
साल 2020 तक, चीन में 5,425 से अधिक ताओबाओ विलेज मौजूद थे, जिन्होंने अनुमानित 100 अरब अमेरिकी डॉलर का ऑनलाइन बिक्री राजस्व उत्पन्न किया (AliResearch, 2021)। इसके अतिरिक्त, स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर और माइक्रोग्रिड लागू किए। नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, विशेषकर सौर मिनी-ग्रिड, ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और बिजली कटौती के प्रति लचीलापन बढ़ाने में मदद की है (Zhang & Long, 2021)।
अनुसंधान से पता चलता है कि ज़ेजियांग और सिचुआन जैसे प्रांतों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क और स्मार्ट ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े ग्रामीण परिवारों की औसत आय 15–25% अधिक है, बनिस्बत उन गाँवों के जो इससे वंचित हैं (Li et al., 2022)। हालाँकि, जातीय अल्पसंख्यकों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने में अभी भी अंतराल बने हुए हैं।
अफ्रीका: ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल समावेशन
उप-सहारा अफ्रीका में, जहाँ 50% से अधिक ग्रामीण आबादी के पास विश्वसनीय बिजली तक पहुँच नहीं है (IEA, 2022), वहाँ विकेंद्रीकृत स्मार्ट अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्या का M-KOPA मॉडल अंतिम छोर तक ऊर्जा पहुँच का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यह पे-एज़-यू-गो सोलर किट्स और IoT-सक्षम मीटरों का उपयोग करके ग्रामीण परिवारों को किफायती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराता है (GSMA, 2021)। वर्ष 2021 तक, M-KOPA ने 10 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा, जिससे मिट्टी के तेल के उपयोग और उससे जुड़े कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।
इसी प्रकार, रवांडा का स्मार्ट विलेज कार्यक्रम ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा को ई-हेल्थ और कृषि प्रसार हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत करता है। विश्व बैंक (2021) के अनुसार, रवांडा सरकार ने 300 से अधिक माइक्रोग्रिड स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं। इन्हें प्रायः वाई-फाई हॉटस्पॉट और मोबाइल मनी समाधान के साथ जोड़ा जाता है ताकि स्थानीय उद्यमियों को समर्थन मिल सके।
इल्स्कोग और क्जेलस्ट्रॉम (2021) के एक अध्ययन में पाया गया कि विकेंद्रीकृत, स्मार्ट ऑफ-ग्रिड समाधानों ने पूर्वी अफ्रीकी समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार किया है, क्योंकि इससे समय की बचत हुई, गरीबी में कमी आई और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन मिला। हालाँकि, उच्च प्रारंभिक लागत और सीमित स्थानीय तकनीकी क्षमता के कारण सततता चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।
भारत के लिए प्रमुख सबक
इन वैश्विक उदाहरणों से भारत की स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना यात्रा के लिए तीन महत्वपूर्ण सबक सामने आते हैं:
i. समग्र डिज़ाइन (Integrated Design): सफल मॉडल अनेक सेवाओं जैसे ऊर्जा, ब्रॉडबैंड, गतिशीलता, स्वास्थ्य और शिक्षा को अलग-अलग न मानकर एकीकृत रूप में जोड़ते हैं। भारत के पायलट स्मार्ट विलेज मॉडल्स को भी इसी तरह भारतनेट, पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को अपने स्थानीय विकास योजनाओं में समेकित करना चाहिए।
ii. स्थानीय नवाचार पारितंत्र (Local Innovation Ecosystems): ग्राम पंचायतों और स्थानीय उद्यमियों को समाधान सह-निर्माण के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। यूरोप के स्मार्ट विलेज और चीन के टाओबाओ विलेज दिखाते हैं कि जब निचले स्तर पर नवाचार को डिजिटल उपकरणों और सूक्ष्म-वित्त पोषण का समर्थन मिलता है, तो वह स्थिरता को आगे बढ़ाता है।
iii. लचीलापन और किफ़ायतीपन (Resilience and Affordability): स्मार्ट प्रणालियों को जलवायु और आर्थिक लचीलेपन के अनुरूप डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अफ्रीका के पे-एज़-यू-गो मॉडल्स और चीन के स्मार्ट ग्रिड्स यह दर्शाते हैं कि लचीली और विकेंद्रीकृत तकनीकें गरीबतम परिवारों तक अवसंरचना को पहुँचाने में सक्षम हैं।
iv. अमृत काल 2047 की दृष्टि की ओर अग्रसर भारत इन सबक़ों को अपनाकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि ग्रामीण अवसंरचना केवल विस्तारित ही न हो, बल्कि दीर्घकालीन उपयोगिता, लचीलापन और स्थिरता के साथ तैयार भी हो।
नीतिगत कमियाँ और चुनौतियाँ
हालाँकि भारत के स्मार्ट ग्रामीण अवसंरचना विकसित करने के प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी नीतिगत डिज़ाइन, क्रियान्वयन और दीर्घकालिक स्थिरता के मामले में कई महत्वपूर्ण कमियाँ बनी हुई हैं।
विखंडन और अभिसरण की कमी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), भारतनेट और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं ने अलग-अलग स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्थित अभिसरण (convergence) की कमी के कारण अक्सर निवेश की पुनरावृत्ति या सेवाओं में अंतराल रह जाते हैं (नीति आयोग, 2021)। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को आगे बढ़ाने का प्रयास कई योजनाओं को संरेखित करने के उद्देश्य से है; हालाँकि, क्षमता संबंधी सीमाएँ कई राज्यों में इनके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालती हैं (MoPR, 2023)।
वित्तीय बाधाएँ और संचालन एवं रखरखाव (O&M): एक आवर्ती चुनौती जीवन-चक्र लागत निर्धारण और टिकाऊ संचालन एवं रखरखाव (O&M) फंडिंग पर सीमित जोर है। उदाहरण के लिए, एशियाई विकास बैंक (ADB) की 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि यद्यपि PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का व्यापक निर्माण हुआ है, फिर भी लगभग 30% सड़कों को पाँच वर्षों के भीतर बड़े मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है, जिसका कारण कमजोर रखरखाव बजट और ठेकेदारों की अपर्याप्त दिशा-निर्देश एवं निगरानी है (ADB, 2022)। इसी तरह, JJM के अंतर्गत घर-घर नल जल कनेक्शन की स्थिरता गाँव स्तर पर O&M संरचनाओं पर निर्भर करती है, जो अभी भी कई ग्राम पंचायतों में प्रारंभिक अवस्था में हैं (MoJS, 2023)।
जलवायु लचीलापन की कमी: ग्रामीण अवसंरचना परिसंपत्तियाँ तेजी से चरम मौसम घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो रही हैं। विश्व बैंक (2021) के अनुसार, भारत को बाढ़ और चक्रवातों से ग्रामीण अवसंरचना को हुए नुकसान से प्रतिवर्ष लगभग 5–6 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान होता है। यद्यपि PMGSY-III और जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देश अब जलवायु-लचीले डिज़ाइन को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इनका क्रियान्वयन अभी भी सीमित है (ADB, 2022)। छोटे किसान, महिलाएँ और हाशिए पर खड़े समूह अक्सर इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
डिजिटल विभाजन और कौशल अंतर: हालाँकि भारतनेट ने ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार किया है, लेकिन डिजिटल विभाजन अब भी मौजूद है। TRAI (2024) की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि केवल 37% ग्रामीण परिवारों के पास कार्यात्मक इंटरनेट कनेक्शन है, और महिलाओं तथा बुजुर्ग आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता अब भी कम है (Mehta et al., 2023)। सामुदायिक प्रशिक्षण के बिना, ई-गवर्नेंस और स्मार्ट सेवा वितरण मॉडल अपने लक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाएंगे।
सिफ़ारिशें: उपयोगिता-उन्मुख, लचीली और सतत ग्रामीण अवसंरचना की ओर
इन अंतरालों को दूर करने के लिए लचीलापन, स्थिरता और समावेशी शासन पर आधारित एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक है। वैश्विक श्रेष्ठ उदाहरणों और भारत के अपने पायलट प्रोजेक्ट्स से सीख लेते हुए निम्नलिखित नीतिगत उपाय सुझाए जाते हैं:
स्थानीय योजनाओं के माध्यम से अभिसरण का संस्थानीकरण: GPDP ढांचे पर आधारित होकर, सभी ग्रामीण अवसंरचना निवेश सड़क, जलापूर्ति, ऊर्जा और डिजिटल सेवाएँ को व्यवस्थित रूप से ब्लॉक और जिला-स्तरीय एकीकृत अवसंरचना विकास योजनाओं (IIDPs) के माध्यम से संरेखित किया जाना चाहिए (MoPR, 2023)। इससे पुनरावृत्ति समाप्त करने, धनराशि को एकत्रित करने और केंद्र तथा राज्य योजनाओं के बीच तालमेल का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय सबक: यूरोपीय संघ का LEADER कार्यक्रम और स्मार्ट विलेजेस दृष्टिकोण दर्शाता है कि स्थानीय एक्शन समूह किस प्रकार एकीकृत ग्रामीण परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन में मूल्यवान भूमिका निभा सकते हैं (Dax et al., 2019)।
जलवायु लचीलापन मानकों को मजबूत करना: सरकार को केवल चुनिंदा पायलट प्रोजेक्ट्स तक ही नहीं बल्कि सभी नई ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं तक अनिवार्य जलवायु जोखिम आकलन और लचीले डिज़ाइन मानकों का विस्तार करना चाहिए। सड़कों के लिए इसमें बाढ़-प्रतिरोधी तटबंध, जैव-इंजीनियर्ड ढलान और जलवायु-लचीली सामग्री शामिल हो सकती हैं (ADB, 2022)। जलापूर्ति के लिए सामुदायिक-नेतृत्व वाले वाटरशेड प्रबंधन से स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है (MoJS, 2023)।
अंतरराष्ट्रीय सबक: बांग्लादेश और वियतनाम में, ग्रामीण सड़कों के सामुदायिक-आधारित जलवायु-सुरक्षण ने परिसंपत्तियों के नुकसान को 25% तक कम किया है (World Bank, 2021)।
जीवन-चक्र फंडिंग और O&M को प्राथमिकता देना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियाँ लंबे समय तक कार्यशील बनी रहें, राज्य सरकारों को ग्रामीण सड़कों, जलापूर्ति और डिजिटल अवसंरचना के संचालन एवं रखरखाव (O&M) के लिए समर्पित बजट आवंटित करना चाहिए। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और सामुदायिक सह-वित्त पोषण मॉडल जैसे केन्या में पे-एज़-यू-गो माइक्रोग्रिड्स वित्तीय स्थिरता को बेहतर बना सकते हैं (GSMA, 2021)।
ग्रामीण डिजिटल क्षमता का निर्माण: डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए केवल फाइबर बिछाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता, सस्ते उपकरण और स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा देना होगा। सामुदायिक वाई-फाई, डिजिटल स्किलिंग सेंटर और ग्रामीण टेक स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन को भारतनेट और डिजिटल इंडिया ढांचे के माध्यम से विस्तारित किया जाना चाहिए (TRAI, 2024; Mehta et al., 2023)।
अंतरराष्ट्रीय सबक: चीन के ताओबाओ विलेजेस दिखाते हैं कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को ई-कॉमर्स माइक्रो-उद्यम चलाने का प्रशिक्षण देकर स्थानीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है (Zhou et al., 2020)।
आउटकम-आधारित निगरानी को बढ़ावा देना: अंततः केवल परिसंपत्ति निर्माण से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित निगरानी को अपनाना आवश्यक है। प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) में केवल सड़कों की लंबाई या नल कनेक्शनों की संख्या नहीं, बल्कि सेवा की उपलब्धता, जलवायु लचीलापन, उपयोगकर्ता संतुष्टि और गरीबी पर प्रभाव जैसे संकेतकों को भी शामिल किया जाना चाहिए (NITI Aayog, 2021)।
निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्ग
उपयोगिता-आधारित, लचीली और सतत ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण भारत के विकास लक्ष्यों और अमृत काल की परिकल्पना को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही भारत एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) तथा एसडीजी 11 (सतत शहर और समुदाय) की ओर बढ़ रहा है, नीतिगत बदलाव का रुख खंडित, अल्पकालिक परियोजनाओं से हटकर एकीकृत, जीवन-चक्र-आधारित निवेशों की ओर होना चाहिए, जिससे ग्रामीण समुदाय बदलते जलवायु और डिजिटल अर्थव्यवस्था में फल-फूल सकें।
यूरोपीय संघ, चीन और अफ्रीका से प्राप्त सबक स्पष्ट करते हैं कि स्थानीय नवाचार, जलवायु लचीलापन और सामुदायिक स्वामित्व सफलता के अटूट स्तंभ हैं। व्यवस्थित अभिसरण, पर्याप्त वित्तपोषण और डिजिटल एवं जलवायु तैयारी को बढ़ावा देकर भारत सुनिश्चित