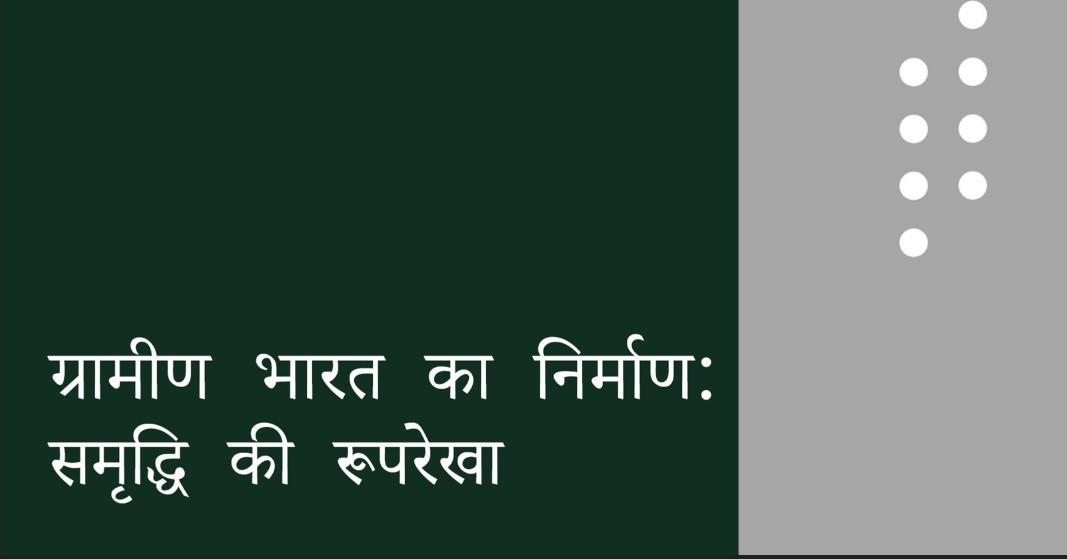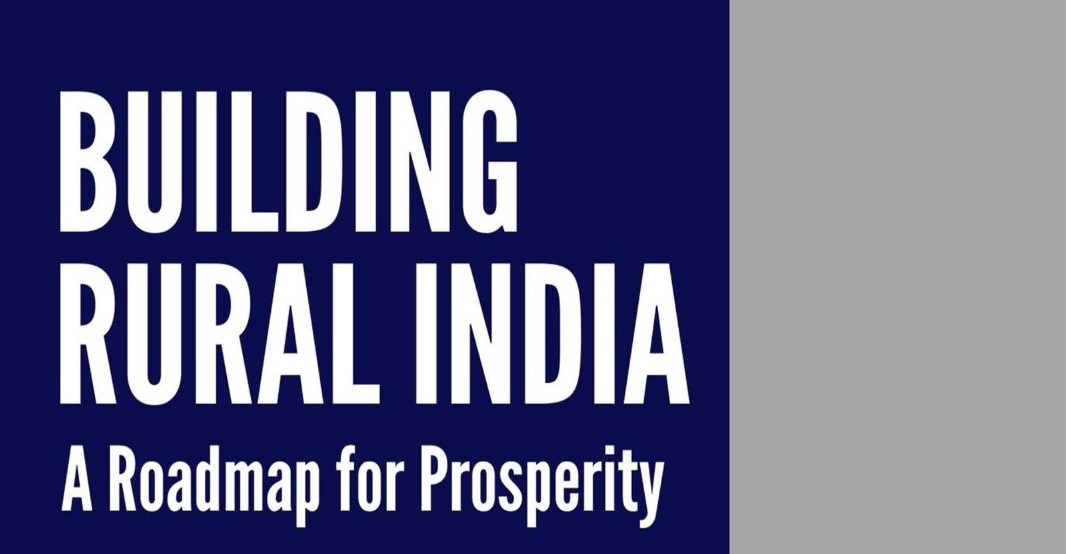ग्रामीण आजीविकाओं का भविष्य कृषि से परे
सारांश
ग्रामीण आजीविकाओं का रूपांतरण केवल एक आर्थिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकता भी है। ऐसा ग्रामीण अर्थतंत्र, जो सम्मानजनक, विविधीकृत और सतत् रोजगार उपलब्ध कराए, समावेशी विकास का मूल आधार है। कृषि से आगे बढ़ने का अर्थ इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इस पर आधारित होकर एक सशक्त और भविष्य के लिए तैयार ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। इसके लिए गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार के प्रमुख अवसरों जैसे डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था, ग्रामीण बीपीओ, लॉजिस्टिक्स में ग्रामीण आजीविकाएँ, हरित रोजगार और कृषि-तकनीक सेवाएँ को खोजना आवश्यक है। भारत के पास डिजिटल संपर्क और हरित परिवर्तन के दोहरे इंजनों के माध्यम से इस भविष्य का निर्माण करने का ऐतिहासिक अवसर है। लोगों, संस्थानों, प्लेटफ़ॉर्मों और साझेदारियों में निवेश करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारे गाँव संकट का प्रतीक न बनें, बल्कि संभावनाओं का केंद्र बनें।
मुख्य शब्द: गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण बीपीओ, डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स में अवसर, हरित रोजगार, कृषि-तकनीक सेवाएँ, सुरक्षा जाल, सहायक परिवेश और श्रम उत्पादकता।
परिचय
भारत, जिसकी जड़ें गहराई से उसके गाँवों में बसी हैं, ने ऐतिहासिक रूप से अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि के पर्याय के रूप में देखा है, जहाँ ग्रामीण आजीविकाएँ मुख्यतः कृषि पर निर्भर रही हैं। यह क्षेत्र देश की कुल कार्यशक्ति का 45.5 प्रतिशत, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60 प्रतिशत, और 83 प्रतिशत ताजे जल संसाधनों का उपयोग करता है, फिर भी यह केवल 15.1 प्रतिशत सकल मूल्य वर्धन (GVA) में योगदान देता है। इसका स्पष्ट संकेत है कि भारत में कृषि श्रम उत्पादकता केवल 20.5 प्रतिशत है, जबकि गैर-कृषि क्षेत्रों में यह कहीं अधिक है। भारत 1.40 अरब लोगों का पेट भरने के बाद भी एक शुद्ध खाद्य निर्यातक देश है, फिर भी किसानों की आय स्तर समान रूप से नहीं बढ़ पाई है। यह परिस्थिति ग्रामीण आर्थिक संरचना में बड़े बदलाव की आवश्यकता के प्रबल संकेत देती है।
भारत की कृषक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन
भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि का हिस्सा 1950-51 में 52 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 14.7 प्रतिशत रह गया है (चार्ट-3.1)। यह आर्थर लुईस के परिकल्पना का समर्थन करता है कि आर्थिक विकास के साथ GDP में कृषि का हिस्सा निरंतर घटता जाता है।
भूमि जोतों का विखंडन
उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक भूमि, वर्षों के दौरान लगातार विखंडित होती जा रही है (चार्ट-3.2), जिसका मुख्य कारण अधिक संख्या में एकल (न्यूक्लियर) परिवारों का बनना है। औसत भूमि जोत का आकार 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में आधे से भी कम यानी 1.08 हेक्टेयर रह गया है। इसका किसानों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह ग्रामीण आजीविका के वैकल्पिक साधनों की खोज की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
भारत में 1990 के दशक में जब एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधार लागू किए गए, तब ये सुधार अर्थव्यवस्था के तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों में तो शुरू किए गए, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को इन सुधारों से अलग रखा गया। तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों में किए गए सुधारों के लाभ धीरे-धीरे ही प्राथमिक क्षेत्र तक पहुँचते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे नीचे, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) बीच में और सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर स्थित होता है। यदि सुधारों की तुलना रॉकेट प्रक्षेपण से की जाए, तो इन्हें ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ही आरंभ और प्रक्षेपित किया जाना चाहिए था।
Chart-3.3: Contrasting Approaches to Reforms, India & China
ग्रामीण भारत का बदलता परिदृश्य: रुझान और अवसर
भारत की ग्रामीण जनसांख्यिकी में समय के साथ धीरे-धीरे लेकिन उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जो जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यद्यपि भारत अब भी मुख्यतः ग्रामीण है, फिर भी ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा दशकों से लगातार घटता जा रहा है।
पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिले हैं, जिन्होंने नए आजीविका मॉडल की नींव रखी है और प्रगति के साथ-साथ बनी हुई चुनौतियों को भी उजागर किया है।
जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक संक्रमण
भारत में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 1951 में 82.7 प्रतिशत से घटकर 2011 में 68.8 प्रतिशत रह गया। कुल कार्यबल में से 72.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता था। वर्षों से लगातार हो रहे शहरीकरण ने देश की जनसंख्या, कार्यबल और जीडीपी में ग्रामीण हिस्सेदारी में गिरावट ला दी है। 1951 से 2011 के बीच कुल जनसंख्या 3.35 गुना बढ़ी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या केवल 2.78 गुना ही बढ़ी। यह दर्शाता है कि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही और शहरीकरण की प्रवृत्ति लगातार बनी रही, भले ही वह धीमी गति से क्यों न हो। अनुमानों के अनुसार, भारत कम से कम 2050 तक प्रमुख रूप से ग्रामीण ही रहेगा, जिसके बाद शहरी जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या से अधिक होने का अनुमान है। यह जनसांख्यिकीय वास्तविकता राष्ट्रीय विकास की कहानी में ग्रामीण भारत के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है। आने वाले दशकों तक ग्रामीण क्षेत्र विशाल कार्यबल का घर बने रहेंगे, जिसके लिए इन क्षेत्रों में सुदृढ़ आजीविका रणनीतियों की आवश्यकता होगी।
सामाजिक-आर्थिक संकेतक भी एक मिश्रित लेकिन सामान्यतः सुधारित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो विभिन्न विकास पहलों के प्रभाव को दर्शाते हैं।
साक्षरता: ग्रामीण भारत में साक्षरता, यद्यपि अब भी शहरी क्षेत्रों से पीछे है, फिर भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। 1951 में ग्रामीण साक्षरता मात्र 12.1% थी, जो उस समय की शहरी दर का लगभग एक-तिहाई थी। 2011 तक यह बढ़कर 68.9% हो गई, जिससे अंतर काफी कम हुआ। हालांकि, यह तथ्य कि ग्रामीण जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई अब भी निरक्षर है, एक स्थायी चुनौती को उजागर करता है, जिसे समान आजीविका विविधीकरण के लिए दूर करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में लैंगिक असमानता भी मौजूद है। 2011 में ग्रामीण पुरुष साक्षरता 80.88% थी जबकि ग्रामीण महिला साक्षरता 64.63% रही। यह अंतर लक्षित हस्तक्षेपों की मांग करता है, क्योंकि शिक्षित महिलाएँ परिवार की भलाई और विविध क्षेत्रों में आर्थिक भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।
स्वास्थ्य: सकल जन्म दर, सकल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे संकेतकों में ग्रामीण-शहरी अंतर लगातार कम होता गया है, विशेषकर 1991 के बाद से। जीवन प्रत्याशा भी दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है 1951 में यह 32.1 वर्ष थी, जो 2011 में बढ़कर 67 वर्ष हो गई और 2030 तक 73.6 वर्ष होने का अनुमान है। विकास के सामाजिक आयामों में यह प्रगति एक स्वस्थ और संभावित रूप से अधिक उत्पादक कार्यबल तैयार करती है, जो अधिक कठिन और कुशल गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम है। बेहतर स्वास्थ्य परिणाम वेतन हानि और बीमारियों पर घरेलू व्यय को भी कम करते हैं, जिससे शिक्षा या छोटे व्यवसायों में निवेश के लिए संसाधन मुक्त हो पाते हैं।
आय और उपभोग: ग्रामीण आय, शहरी प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में, कुछ हद तक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाती है, लेकिन 1999-2000 के बाद इसमें सुधार देखा गया। प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है 1950-51 में यह ₹265 थी, जो 2010-11 में ₹56,971 और 2020-21 में ₹1,28,829 (वर्तमान मूल्यों पर) हो गई। 2011-12 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक घरेलू व्यय शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जिससे उपभोग में असमानताएँ कम हुई हैं। यह ग्रामीण क्रय शक्ति में सुधार का संकेत देता है, जो आगे चलकर ग्रामीण बाज़ारों में गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं की माँग को बढ़ा सकता है तथा स्थानीय उद्यमशील अवसर पैदा कर सकता है।
गरीबी में कमी: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा (रंगराजन समिति की पद्धति के अनुसार) 2011-12 में ₹972, 2022-23 में ₹1,837 और 2023-24 में ₹1,940 रही। शहरी क्षेत्रों के लिए यह क्रमशः ₹1,407 (2011-12), ₹2,603 (2022-23) और ₹2,736 (2023-24) रही।
तालिका-3.1: ग्रामीण बनाम शहरी गरीबी रेखा, 2011-12 से 2023-24 तक
Note: Based on Rangarajan Committee
2023-24 के दौरान ग्रामीण गरीबी, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी हो गई। चूँकि ‘सुरक्षा जाल’ (कल्याणकारी कार्यक्रमों) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई नहीं देता, इसलिए 2023-24 में गरीबी में कमी का निकटतम कारण ‘जीडीपी वृद्धि’ हो सकता है (रंगराजन, 2025)
गरीबी का स्वरूप और कारण
गरीबी के स्वरूप और कारणों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है ‘भौगोलिक गरीबी’ और ‘परिवारगत गरीबी’। भौगोलिक गरीबी उन अविकसित क्षेत्रों से जुड़ी होती है जहाँ अवसंरचना, सेवाओं और आर्थिक अवसरों की कमी होती है। यह अक्सर ऐतिहासिक उपेक्षा या पर्यावरणीय बाधाओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए, राजीव चौक और हौज खास (नई दिल्ली) में एक मोची प्रतिदिन लगभग ₹2650 कमाता है, जबकि उदलगुरी (उत्तर असम) में उसका समकक्ष केवल ₹105 प्रतिदिन ही कमा पाता है। परिवारगत गरीबी का संबंध व्यक्तिगत परिवारों से होता है, जो भोजन, पोषण, आश्रय, लगातार कमजोर शिक्षा, कम कौशल स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं। जहाँ भौगोलिक गरीबी स्थानिक और प्रणालीगत होती है, वहीं परिवारगत गरीबी व्यक्तिगत और तात्कालिक होती है। सामाजिक बहिष्कार और पर्यावरणीय क्षरण गरीबी को और भी जटिल बना देते हैं। ये आपस में जुड़े कारण दर्शाते हैं कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि संरचनात्मक और सामाजिक कमियों में भी निहित है, जिसके लिए स्थायी उन्मूलन हेतु व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। दोनों तरह की गरीबी को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और वंचित परिवारों के सशक्तिकरण पर लक्षित ध्यान देना जरूरी है, ताकि वंचना के इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सके।
Chart-3.4: Causes of Poverty
ग्रामीण असमानता
जिनी गुणांक, जो असमानता का एक माप है, 2011-12 से 2022-23 और फिर 2022-23 से 2023-24 के दौरान देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में घटा है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी असमानता कम हुई है, लेकिन इसकी गति शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ धीमी रही है (चार्ट-3.5)
ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता में गिरावट 2022-23 से 2023-24 के बीच केवल एक वर्ष में 0.029 अंकों की रही, जबकि 2011-12 से 2022-23 के 11 वर्षों की अवधि में यह गिरावट मात्र 0.017 अंकों की थी। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में यह गिरावट क्रमशः 0.030 और 0.049 अंकों की रही।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण
ग्रामीण परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण और आशाजनक बदलाव इसकी अर्थव्यवस्था का धीरे-धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से हो रहा संरचनात्मक रूपांतरण है, जिसमें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता से हटकर एक अधिक विविधीकृत आधार की ओर रुख किया जा रहा है। ग्रामीण भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1970-71 में 72.4% से घटकर 2011-12 में 39% रह गई (चंद, 2022)। ग्रामीण उत्पादन में कृषि के योगदान में यह तेज गिरावट, भले ही यह अब भी एक बड़े कार्यबल का सहारा बना हुआ है, इस क्षेत्र की उच्च-मूल्य रोजगार उत्पन्न करने की घटती क्षमता को दर्शाती है। इसी अवधि में ग्रामीण NDP में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी तीन गुना से अधिक बढ़ गई, जो 1970-71 में 10.6% से बढ़कर 2011-12 में 32.2% हो गई। सेवाओं के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसकी हिस्सेदारी इसी अवधि में 17.1% से बढ़कर 28.8% तक पहुँच गई। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों की ओर एक स्पष्ट और स्थायी बदलाव हो रहा है।
इस रूपांतरण की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ग्रामीण भारत एक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) के रूप में उभर रहा है। 1970-71 में ग्रामीण क्षेत्रों का कुल विनिर्माण NDP में योगदान मात्र एक-चौथाई था। 2011-12 तक यह हिस्सा बढ़कर आधे से अधिक (51.3%) हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि विनिर्माण इकाइयाँ बढ़ती हुई संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों को आकर्षक पा रही हैं, जिसका कारण है – कम भूमि लागत, श्रम की उपलब्धता, और भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर नियामक वातावरण।
हाल के रुझानों का उलटाव: बढ़ता ग्रामीण कार्यबल और आर्थिक गतिविधियों का स्थानांतरण
एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास ग्रामीण रोजगार में 2017-18 के बाद देखा गया "टर्नअराउंड" है। अतीत के उन रुझानों के विपरीत, जिनमें कुल रोजगार में ग्रामीण हिस्सेदारी घट रही थी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़े ग्रामीण कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। 2017-18 से 2022-23 के बीच ग्रामीण कार्यबल में प्रतिवर्ष 5.16% की मजबूत दर से वृद्धि हुई, जबकि शहरी कार्यबल में यह वृद्धि केवल 0.81% रही। इसके परिणामस्वरूप कुल कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2017-18 के 71.4% से बढ़कर 2022-23 में 75.6% हो गई। यह भारत के श्रम बाज़ार की गतिशीलता में शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इस बदलाव के पीछे के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
• सस्ती भूमि की उपलब्धता: ग्रामीण क्षेत्र विनिर्माण इकाइयों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत सस्ती भूमि उपलब्ध कराते हैं, जिससे व्यवसायों की संचालन लागत कम होती है।
• कम मजदूरी: यद्यपि मजदूरी दरें बढ़ रही हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम लागत शहरी केंद्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
• सरकारी प्रोत्साहन: गैर-महानगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन।
• सुधरता अवसंरचना: बेहतर सड़क संपर्क, बिजली की बढ़ती पहुँच और विस्तृत डिजिटल अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्रों को व्यवसायों के लिए अधिक उपयुक्त बना रही है।
• उल्टा पलायन और स्थानीय प्रतिभा: स्थानीय कार्यबल की उपलब्धता, जिसे कभी-कभी शहरों से लौटे कुशल श्रमिकों के उल्टे पलायन से और भी सशक्त किया जाता है, एक तैयार प्रतिभा पूल प्रदान करती है।
यह बदलाव विविधीकृत ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ाने का एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह केवल विवशता से होने वाले पलायन जैसे धकेलने वाले कारकों पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की ओर स्वाभाविक आर्थिक आकर्षण को दर्शाता है।
गैर-कृषि ग्रामीण आजीविकाओं के उभरते मार्ग
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण, जिसका प्रमाण सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि की घटती हिस्सेदारी और विनिर्माण एवं सेवाओं के बढ़ते योगदान से मिलता है, गैर-कृषि रोजगार की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। गैर-कृषि क्षेत्र के भीतर उभरते हुए प्रमुख मार्ग ग्रामीण भारत में विविध और सतत आजीविकाएँ उत्पन्न करने की अपार संभावनाएँ रखते हैं, जिनका आधार तकनीकी प्रगति और ग्रामीण परिवेश की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं।
ग्रामीण बीपीओ का विकास और वितरित डिजिटल कार्य का उदय
बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) की अवधारणा, जो महानगरीय केंद्रों से निकलकर छोटे शहरों और गाँवों तक पहुँची है, भारत में समावेशी विकास और रोजगार सृजन के एक व्यवहार्य मॉडल के रूप में उभर रही है। ग्रामीण भारत में शिक्षित युवाओं का एक विशाल समूह मौजूद है, जिनमें से कई माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। वे रोजगार के अवसरों के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से बड़े शहरों में पलायन करने के इच्छुक या सक्षम नहीं होते। ग्रामीण बीपीओ इन्हें घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराते हैं, इस अप्रयुक्त प्रतिभा का उपयोग करते हैं और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में मजबूरीवश होने वाले पलायन को कम करते हैं।
भारत में बीपीओ की शुरुआत मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे महानगरों में हुई, जहाँ बड़ी संख्या में स्नातक उपलब्ध थे और पश्चिमी देशों की तुलना में श्रम लागत कम थी। इन केंद्रों को कम परिचालन लागत, कम कर्मचारी पलायन दर और ग्रामीण युवाओं की बढ़ती डिजिटल दक्षता (विशेष रूप से भारतनेट और स्मार्टफोन प्रसार के कारण) का लाभ मिला। और जैसे संगठन ग्रामीण प्रतिभा का उपयोग डेटा एंट्री, कंटेंट मॉडरेशन और ग्राहक सेवा जैसी डिजिटल सेवाओं में कर रहे हैं। कुछ बीपीओ केंद्रों में कई प्रथम-पीढ़ी की युवा महिला पेशेवर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और शहरी कंपनियों के लिए बैक-एंड संचालन संभाल रही हैं। हालांकि, शहरी केंद्रों में इनके उल्लेखनीय विस्तार से कई चुनौतियाँ सामने आईं जिनमें प्रतिभा के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा, उच्च कर्मचारी पलायन (अक्सर 30-40% वार्षिक से अधिक), स्टाफ की बार-बार "पोचिंग" और इसके परिणामस्वरूप भर्ती व प्रशिक्षण लागत में वृद्धि शामिल हैं। फिर भी, ग्रामीण बीपीओ की सफलता यह दर्शाती है कि शहरी भारत के बाहर डिजिटल रोजगार की अप्रयुक्त संभावनाएँ मौजूद हैं।
वर्तमान में कई ग्रामीण बीपीओ छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, जिससे वे बड़े और दीर्घकालिक अनुबंध हासिल करने में सीमित हैं। छोटे ग्रामीण संगठनों के लिए विपणन और बिक्री भी चुनौतीपूर्ण होती है। शुरुआती चरण में ग्रामीण बीपीओ को मूल्य श्रृंखला के निचले स्तर पर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में वॉइस-आधारित सेवाएँ, डिजिटलीकरण और डेटा प्रबंधन, जो उनके लिए अत्यंत किफायती हैं। वे एक "नेटवर्क मॉडल" भी अपना सकते हैं, जिसमें कई छोटे ग्रामीण केंद्र आपस में जुड़कर एक बड़े संस्थान की तरह काम करें, या फिर बड़े शहरी केंद्रों में स्थित बीपीओ के सैटेलाइट केंद्र के रूप में कार्य करें।
ग्रामीण बीपीओ आमतौर पर उन सेवाओं को संभालते हैं जो कम जटिल होती हैं या जिनमें स्थानीय भाषा दक्षता की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं: वॉइस-आधारित सेवाएँ, इंटरनेट कंटेंट मॉनेटाइजेशन, सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण, बैक-ऑफिस संचालन, कंटेंट मॉडरेशन और ट्रांसक्रिप्शन, अप्रयुक्त प्रतिभा पूल तक पहुँच, कम कर्मचारी पलायन दर। भारत सरकार ने भी इस विकेंद्रीकरण का सक्रिय समर्थन किया है। “इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम” (IBPS), जिसे 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लगभग ₹500 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किया गया, का विशेष उद्देश्य छोटे शहरों और गाँवों में नए रोजगार अवसर सृजित करना था। इस योजना के तहत गैर-टियर-1 शहरों में बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करने वाली कंपनियों को पूंजीगत व्यय का 50% तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। इस पहल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और अमेज़न जैसे बड़े संगठनों को दूरदराज के क्षेत्रों में संचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित किया।
ग्रामीण क्षेत्रों और व्यवसायों के लिए लाभ
ग्रामीण बीपीओ की स्थापना अनेक लाभ प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण समुदायों और संबंधित कंपनियों दोनों के लिए विन-विन स्थिति बनती है। इनमें शामिल हैं व्यवसायों के लिए अत्यधिक कम परिचालन लागत (नियत लागत और परिवर्ती लागत दोनों), कम कर्मचारी पलायन दर, कम मजदूरी और उपयोगिता खर्च। इसके अतिरिक्त, ये केंद्र आर्थिक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करते हैं क्योंकि ग्रामीण बीपीओ कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती है, जिससे स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ती है। यह बढ़ी हुई क्रय शक्ति स्थानीय बाज़ारों को प्रोत्साहित करती है, छोटे व्यवसायों को सहारा देती है और सहायक सेवाओं जैसे स्थानीय भोजनालयों, परिवहन, कर्मचारियों के लिए आवास आदि की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे सकारात्मक आर्थिक गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि अवसंरचना में निरंतर रणनीतिक निवेश, कौशल विकास पर विशेष ध्यान और सहायक नीतिगत ढाँचे उपलब्ध हों, तो ग्रामीण बीपीओ ग्रामीण भारत में समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उल्टा पलायन को प्रेरित कर सकते हैं और इस प्रकार विविधीकृत आजीविका रणनीति के एक आधारस्तंभ बन सकते हैं।
ग्रीन जॉब्स: ग्रामीण स्थिरता और रोजगार का संगम
पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ, ग्रामीण ग्रीन जॉब्स एक आवश्यकता और अवसर दोनों बनते जा रहे हैं। इनमें सौर ऊर्जा स्थापना, जलग्रहण प्रबंधन, जैविक खेती और एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य मित्रा कार्यक्रम ने हजारों ग्रामीण युवाओं को सोलर पैनल लगाने और उसके रखरखाव का प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से कई अब सोलर पार्कों और रूफटॉप परियोजनाओं में कार्यरत हैं। इसी तरह, मनरेगा (MGNREGA) को भी तेजी से हरित लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है जैसे वनीकरण और जल संरक्षण जिससे स्थायी परिसंपत्तियाँ और रोजगार दोनों सृजित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में 2030 तक 30 लाख से अधिक ग्रीन जॉब्स सृजित करने की क्षमता है, जिनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में होगी।
एग्री-टेक और सेवा-उन्मुख खेती
कृषि स्वयं अब तेजी से सेवा-आधारित होती जा रही है। एग्री-टेक स्टार्टअप्स जैसे DeHaat, CropIn और FASAL एआई-आधारित परामर्श सेवाएँ, इनपुट आपूर्ति और फसल कटाई के बाद सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण युवाओं को ड्रोन ऑपरेटर, फसल निरीक्षक, कृषि परामर्शदाता और लॉजिस्टिक्स स्टाफ के रूप में रोजगार दे रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम जैसे किसान ड्रोन योजना "ड्रोन-एज़-ए-सर्विस" को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ प्रशिक्षित ग्रामीण युवा किसानों को छिड़काव और निगरानी सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये पहलें न केवल रोजगार पैदा करती हैं बल्कि कृषि को अधिक कुशल और डेटा-आधारित भी बनाती हैं।
डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) कौशल में एक बड़ा अंतर है। वर्ष 2020-21 में केवल 18.1% ग्रामीण युवा (15 वर्ष और उससे ऊपर) "कंप्यूटर साक्षर" पाए गए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 39.6% था। यह स्थिति ग्रामीण युवाओं को उद्योग-तैयार बनाने हेतु गहन मौलिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाती है।
समाधान सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निहित है, विशेषकर शिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए, ताकि डिजिटल रोजगार बाजार में उन्हें बराबरी का अवसर मिल सके। इस कौशल अंतर को पाटने के लिए बीपीओ, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक) और सरकारी कौशल विकास मिशन (जैसे स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - PMKVY) के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण का फोकस होना चाहिए: संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर दक्षता, डाटा एंट्री में सटीकता, ग्राहक सेवा शिष्टाचार और सेवाओं से संबंधित डोमेन-विशिष्ट ज्ञान पर। इसके अतिरिक्त, "स्किल बैज" या "स्किल पासपोर्ट" जैसी व्यवस्थाएँ योग्यता को प्रमाणित करने में सहायक हो सकती हैं।
सक्षम वातावरण और ग्रामीण रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र
ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में राज्य की क्षमता और विकेंद्रीकृत शासन के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस आधार पर, निम्नलिखित प्राथमिकताएँ उभरकर सामने आती हैं:
i. ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना।
ii. कार्यक्रमों का एकीकरण और अभिसरण: ग्रामीण रोजगार योजनाओं (मनरेगा), कौशल विकास कार्यक्रमों (DDU-GKY), और जलवायु लक्ष्यों (PM-KUSUM) को बहुआयामी प्रभाव के लिए आपस में जोड़ना।
iii. गिग और असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा: ई-श्र्म पोर्टल का विस्तार कर ग्रामीण गिग श्रमिकों को बीमा और पेंशन योजनाओं में शामिल करना।
iv. एफपीओ और एसएचजी को नियोक्ता के रूप में बढ़ावा देना: वित्त, प्रौद्योगिकी और विपणन में सहयोग देकर इन्हें प्रमुख ग्रामीण रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा सकता है।
इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए मंत्रालयों के बीच नीतिगत समन्वय, डेटा का बेहतर उपयोग और परिणाम आधारित आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।
सरकारी पहल और उनका प्रभाव
ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में देखी गई प्रगति का बड़ा हिस्सा पिछले कई दशकों में किए गए सतत और संगठित सरकारी प्रयासों को श्रेय दिया जा सकता है। इन पहलों ने आधारभूत अवसंरचना तैयार की है, सामाजिक संकेतकों में सुधार किया है और प्रत्यक्ष रूप से आजीविका सृजन का समर्थन किया है।
i. कनेक्टिविटी और अवसंरचना: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने असंलग्न ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्रामीण गरीबी और अलगाव का एक प्रमुख संरचनात्मक कारण संबोधित हुआ है। बेहतर सड़कें कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार तक पहुँच आसान करती हैं, गैर-कृषि व्यवसायों के लिए माल की आवाजाही को सक्षम बनाती हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सेवाओं तक पहुँच को बेहतर करती हैं।
ii. सामाजिक सुरक्षा जाल और वित्तीय समावेशन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति और प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN) के तहत मुफ्त पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने जैसी लक्षित पहलों ने खाद्य सुरक्षा और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता और सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युत आपूर्ति ने ग्रामीण परिवारों में ऊर्जा पहुँच को सुधारा है। जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और जल लाने की कठिनाई कम होगी। औपचारिक वित्तीय सेवाओं के व्यापक विस्तार ने आर्थिक गतिविधियों के औपचारिकीकरण, डिजिटल लेन-देन को सुगम बनाने और ग्रामीण उद्यमियों एवं परिवारों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 50 करोड़ नए बैंक खाते खोलकर यह उपलब्धि हासिल की है।
iii. कौशल विकास और उद्यमिता संवर्धन: सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि ग्रामीण युवाओं की रोजगार-योग्यता को बढ़ाया जा सके। स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) के लिए सहयोग जैसी योजनाएँ ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं। “लखपति दीदी” पहल महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से सशक्त बनाने और उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियाँ हासिल करने में सक्षम बनाने के सरकार के फोकस को दर्शाती है।
हालाँकि इन पहलों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन सार्वजनिक व्यय में “लीकेज” और “राज्य की क्षमता” को मज़बूत करने की आवश्यकता, जैसा कि मुरलीधरन (2024) ने तर्क दिया है, जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जहाँ वित्तीय आवंटन आवश्यक है, वहीं कार्यक्रम व्यय की गुणवत्ता और दक्षता, साथ ही मज़बूत शासन व्यवस्था, भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकें और इन विकास प्रयासों की सततता सुनिश्चित हो सके।
ग्रामीण भारत का बदलता परिदृश्य जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन, संरचनात्मक आर्थिक विविधीकरण, और सरकारी हस्तक्षेपों के सकारात्मक प्रभाव से परिभाषित है गैर-कृषि आजीविका के अवसरों को तलाशने और विस्तार देने के लिए एक उपजाऊ भूमि प्रदान करता है।
संस्थाओं का सशक्तिकरण: पंचायत राज संस्थाएँ
विकेंद्रीकरण, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से, भारत में ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक शासन का आधारस्तंभ है। एक जीवंत और गतिशील स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पंचायतें राज्य की क्षमता निर्माण में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
Chart-3.5: PRIs Functions
विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप शासन प्रणाली में ‘ऊपर से नीचे’ मॉडल से ‘नीचे से ऊपर’ मॉडल की ओर एक भागीदारी आधारित विकास मॉडल में परिवर्तन की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि पंचायत राज संस्थाएँ (PRIs) अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही हैं, फिर भी अधिकांश राज्यों में इन्हें ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों के हस्तांतरण के अभाव में गंभीर सीमाओं का सामना करना पड़ता है। ये कार्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं और इन्हें इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि पंचायत राज संस्थाएँ वास्तविक स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। ग्रामीण भारत में सेवा वितरण में सुधार और विकास एजेंडे के केंद्र में नागरिक-केंद्रितता लाने के लिए, आवश्यक है कि पंचायत राज संस्थाओं को उनके सच्चे स्वरूप में सशक्त किया जाए। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘सूची-IV – पंचायतों और नगरपालिकाओं के अधीन विषयों’ को सम्मिलित कर तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) जैसी समानांतर संस्थाओं को समाप्त करके प्राप्त किया जा स