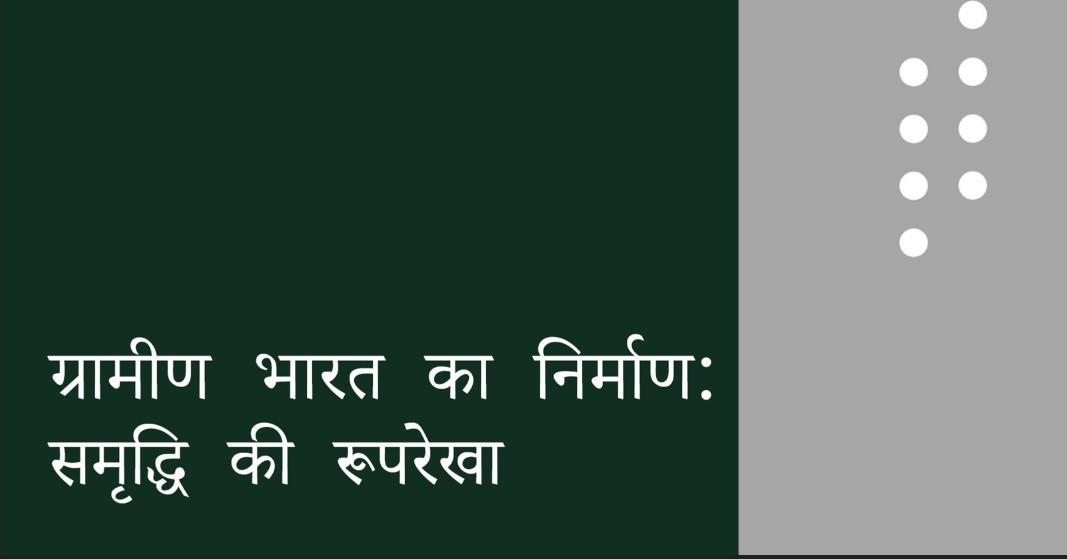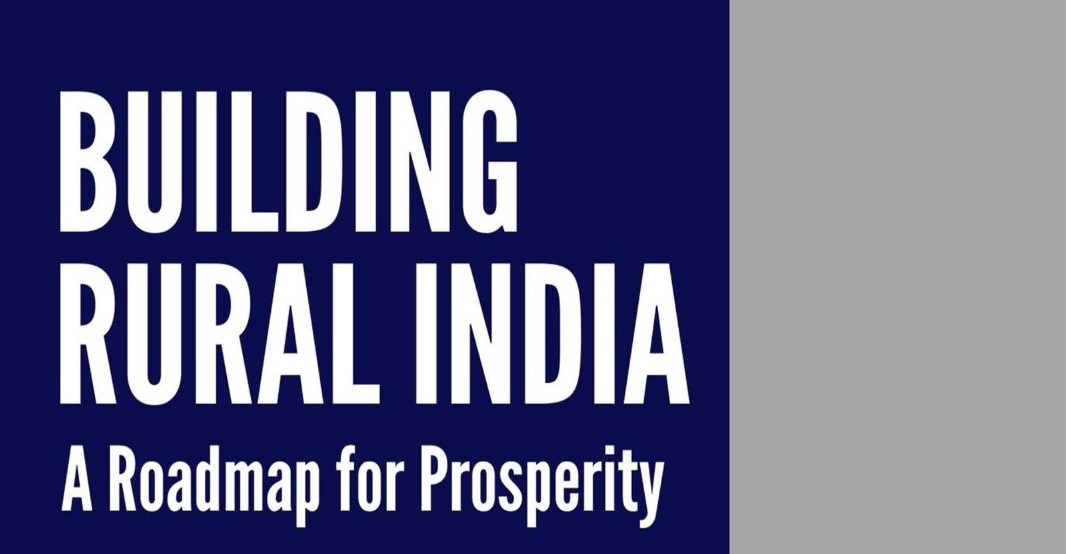भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग के अवसर/विकल्प : राजस्थान पर विशेष ध्यान
सारांश
यह शोधपत्र राज्य स्तर पर जमीनी स्तर के ऐतिहासिक सुधारों की प्रकार्य-विधा तथा राज्य राजस्व मंडल द्वारा आरंभ किए गए विशिष्ट सुधारों का विवेचन करता है। इन सुधारों ने भारत सरकार की अनेक कानूनी सहायता एवं सशक्तिकरण पहलों (जैसे नि:शुल्क विधिक सेवाएँ, टेली-लॉ सेवा और न्याय मित्र योजना) को न्यायिक सुधारों के संदर्भ में उपयुक्त मान्यता दी। प्रकरण निस्तारण में तेजी, डिजिटल सुधार तथा अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता निर्माण को राज्य राजस्व मंडल ने विधिक ढांचे के सहयोग से आगे बढ़ाया, जो भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने हेतु भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 और राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत तैयार किया गया था। इस शोधपत्र में भूमि सुधारों का विश्लेषण बड़े कृषक जिलों, शहरीकृत जिलों तथा आईजीएनपी (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) कमांड क्षेत्र आदि के विशेष संदर्भ में भी किया गया है।
प्रस्तावना – भूमि सुधार
भूमि सुधार सिविल सेवक की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) भारत में भूमि सुधारों की गहन समझ विकसित करती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक आईएएस प्रशिक्षु को ज़िले के प्रशिक्षण-अवधि में भूमि सुधारों से संबंधित एक विस्तृत असाइनमेंट करना होता है, जिसे कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रस्तुत किया जाता है। इस असाइनमेंट के अंतर्गत एक आईएएस अधिकारी भूमि सीमा मामलों, भू-धारण सुधार जिसमें बंटवारा भी शामिल है, भूमि राजस्व एवं राजस्व न्यायालय कार्य, सामुदायिक भूमि का प्रबंधन, देवस्थल भूमि का प्रबंधन, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा जलग्रहण क्षेत्र विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तत्पश्चात् आईएएस अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जिला कलेक्टर तथा राज्य के राजस्व मंडल में सेवा करते हैं।
मेरे प्रशिक्षण काल में, राजस्थान के नागौर ज़िले में रहते हुए मैंने भूमि सुधारों के प्रति गहरा लगाव विकसित किया। मैंने अनेक गाँवों का दौरा किया, तहसील/उपखण्डों में रात्रि प्रवास किया और किसानों, अधिवक्ताओं, पटवारियों, गिरदावरों, तहसीलदारों तथा उपखण्ड अधिकारियों से संवाद स्थापित कर राजस्थान की जटिल भू-धारण व्यवस्थाओं को समझा। इसके बाद मैंने दो बड़े कृषि प्रधान उपखण्डों भीलवाड़ा और निंबाहेड़ा में उपखण्ड अधिकारी के रूप में, दो मरुस्थलीय ज़िलों पाली और जोधपुर में जिला कलेक्टर के रूप में तथा अजमेर में राजस्थान के राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही मैं इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (IGNP) के अतिरिक्त क्षेत्र विकास आयुक्त तथा राजस्थान के जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशक के पद पर भी रहा। भूमि सुधारों से मेरा 14 वर्षों का गहरा जुड़ाव रहा, जिससे मुझे भू-धारण अधिकारों, सामुदायिक भूमि तथा भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन जैसे जटिल मुद्दों की व्यापक समझ मिली। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भू-धारण अधिनियम, 1955 राज्य के हाथों में ऐसे शक्तिशाली साधन हैं, जो भूमि अधिकार और पट्टेदारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
मैंने हजारों किसानों से संवाद किया जो अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। जिनके पास भूमि अधिकार सुरक्षित हैं स्वामित्व या उपयोग वे उसे प्रभावशाली वर्गों से बचा पाते हैं। राज्य का दायित्व है कि भूमि अधिकारों की रक्षा करे और पट्टेदारी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मुझे 1992 में किए गए अपने अध्ययन की याद आती है, जो उदयपुर ज़िले की झाड़ोल और कोटड़ा तहसीलों में आदिवासी भूमि-अधिग्रहण पर केंद्रित था। इसमें मैंने पाया कि उदयपुर के आदिवासी महाजनों (साहूकारों) से अत्यधिक ब्याज पर कर्ज लेकर भूमि से वंचित हो रहे थे।
राजस्थान के राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में, मैंने राज्य के राजस्व न्यायालयों को न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने, डिजिटलीकरण अपनाने, निर्णय लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा नीति-हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए मार्गदर्शन दिया ताकि बालिकाओं के अधिकार, देवस्थल भूमि, सामुदायिक भूमि और लाखों पट्टेदारों के अधिकार संरक्षित रह सकें।
वर्ष 2014 से 2025 के दौरान, देश ने ग्रामीण परिवर्तन का साक्षी बना। जनधन आधार भीम (JAM) अनुप्रयोगों के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ। राजस्थान की राजस्व प्रशासन ने यह प्रयास किया कि जिन पट्टेदारों के भूमि अधिकार सुरक्षित हैं, उन्हें भूमि में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए बेहतर बीज, मृदा सुधार, सिंचाई आदि के रूप में ताकि इन निवेशों पर हुआ व्यय कृषि उत्पादकता और उपज में वृद्धि कर सके। 2047 तक नए भारत की यात्रा इस पर निर्भर करेगी कि राज्य की राजस्व प्रशासनिक प्रणाली भूमि सुधारों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है।
21वीं सदी में भूमि सुधार
वर्तमान प्रशासन में भूमि सुधारों के क्षेत्र में बड़े संरचनात्मक सुधारों की परिकल्पना की गई है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
1. विभिन्न विभागों में भूमि अभिलेखों का एकीकृत मानक प्रारूप में डिजिटलीकरण।
2. भूमि संबंधी मुकदमों का पुनर्गठन, समय-सीमा में कमी तथा त्वरित न्यायालयों और न्यायिक प्रक्रियाओं की स्थापना।
3. स्टाम्प शुल्क का तार्किक निर्धारण तथा स्टाम्प शुल्क के बोझ को कम करना।
4. संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को सुगम बनाना और भूमि अभिलेखों को स्टाम्प पंजीकरण से जोड़ना।
5. सरकारी आँकड़ों एवं भूमि संबंधी अन्य जानकारियों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना।
किसान के लिए भूमि को गिरवी के रूप में उपयोग करने हेतु समय पर और अद्यतन भूमि अभिलेख अत्यंत आवश्यक हैं। बैंकों द्वारा कृषि ऋण चाहे अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक भूमि को गिरवी रखने पर ही आधारित होते हैं। भूमि अभिलेखों में समय पर म्यूटेशन और अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियाँ न होने की स्थिति में किसानों की ऋण तक पहुँच सीमित हो जाती है।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 98.5 प्रतिशत भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण हो चुका है, किंतु पाठ्य एवं भौगोलिक अभिलेखों में अभी भी अंतर मौजूद है। प्रयास यह है कि उच्च गुणवत्ता वाले भूमि अभिलेख तैयार हों और एक पारदर्शी, आधुनिक भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाए।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य – भूमि संसाधन विभाग की पहलें
भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख पहलें और कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
• डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम – भूमि अभिलेखों एवं पंजीकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण हेतु यह कार्यक्रम 2016-17 से एक केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम के रूप में 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं अधिकार अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण, भू-मानचित्रों का डिजिटलीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, उप-पंजीयक कार्यालयों और तहसीलों के बीच संपर्क स्थापित करना तथा भूमि अभिलेख और पंजीकरण का एकीकरण।
• यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) या भू-आधार – यह प्रत्येक भू-खण्ड के लिए 14 अंकों का अल्फ़ा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान क्रमांक है, जो उस भू-खण्ड के भू-निर्देशांक पर आधारित है।
• राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) – दस्तावेज़ों/विलेखों के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए “One Nation – One Registration” सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे पूरे भारत के पंजीकरण विभागों में लागू किया गया है। इस अभिनव पहल को वर्ष 2021 में नवाचार-केन्द्रीय श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ। NGDRS से संबंधित आंकड़े NGDRS पोर्टल (www.ngdrs.gov.in) पर वास्तविक समय में उपलब्ध हैं।
• राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली – इसे 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
• राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान प्रणाली (NAKSHA) – यह शहरी आबादी क्षेत्रों के भूमि सर्वेक्षण पर आधारित एक रूपांतरणकारी पायलट कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना है।
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2016 से पुनर्गठित कर केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह कार्यक्रम भूमि विवादों को कम करने, बेनामी लेन-देन पर रोक लगाने और वास्तविक समय (Real-Time) में सूचना साझा करके राजस्व कार्यालयों के भौतिक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। DILRMP के अंतर्गत: 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 93% से अधिक अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया गया है। 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक भू-मानचित्र का डिजिटलीकरण किया गया है। 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 93% से अधिक पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 99% से अधिक उप-पंजीयक कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण हो चुका है। अगले चरण में आधार संख्या को भूमि अभिलेख डाटाबेस से जोड़ना, राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा उन्हें भूमि अभिलेखों से एकीकृत करना शामिल है।
ई-कोर्ट को भूमि अभिलेख एवं पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने का उद्देश्य न्यायालयों को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और अंततः भूमि विवादों में कमी आए। RCMS न्यायालयों को अधिकार अभिलेखों, भू-मानचित्रों (जिसमें भू-संदर्भित और पुराने डेटा शामिल हैं) के वास्तविक एवं प्रामाणिक साक्ष्य की प्रथम-हस्त जानकारी उपलब्ध कराता है।
राजस्थान के महत्वपूर्ण भूमि कानून
राजस्थान के भूमि सुधारों से जुड़े प्रमुख कानून हैं:
1. राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 यह एक प्रगतिशील कानून है, जिसमें पट्टेदारों की सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के कई प्रावधान हैं। इस अधिनियम के तहत भूमि स्वामी राज्य है, जिसका प्रतिनिधित्व तहसीलदार करता है। राज्य के दो प्रकार के पट्टेदार हैं खातेदार और गैर-खातेदार।
2. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 यह एक समेकित और संशोधन अधिनियम है, जो भूमि, भू-राजस्व, राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कर्तव्यों तथा भूमि अभिलेखों की तैयारी से संबंधित प्रावधान करता है। जिला कलेक्टर की शक्तियाँ मुख्य रूप से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न भूमि आवंटन नियमों से प्राप्त होती हैं।
भूमि सुधार – राजस्व कानूनों के मुख्य प्रावधान
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराएँ, जो राजस्व मंडल (Board of Revenue) से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं:
1. धारा 4 – मंडल की स्थापना एवं संरचना : राजस्थान का राजस्व मंडल एक अध्यक्ष और 20 सदस्यों से मिलकर गठित होगा।
2. धारा 5 – सदस्यों का कार्यकाल : मंडल के सभी सदस्य राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।
3. धारा 6 – बैठक का स्थान : राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर होगा, किंतु राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा मंडल अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी स्थान पर बैठ सकता है।
4. धारा 7 – मंत्रालयिक अधिकारी : राजस्व मंडल के मंत्रालयिक अधिकारी रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा 3 उप-रजिस्ट्रार होंगे। इन्हें मंडल द्वारा निर्देशित शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी और वही कार्य संपादित करेंगे।
5. धारा 8 – मंडल की शक्तियाँ : राजस्व मंडल राजस्थान का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है, जो अपील, पुनरीक्षण और संदर्भ (Appeal, Revision, Reference) के मामलों में अधिकार रखता है। मंडल की तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं – (a) अपील (Appeal) (b) पुनरीक्षण (Revision) (c) संदर्भ (Reference)
ये शक्तियाँ निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन प्रयोग की जाती हैं:
a. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 74 से 87 : अपील, पुनरीक्षण, संदर्भ और पुनर्विचार के लिए, धारा 53 से 55 : प्रकरणों के स्थानांतरण और एकीकरण के लिए, धारा 261(1) : अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए।
b. राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955-धारा 222 से 228 : अपीलों के लिए, धारा 230 से 231 : पुनरीक्षण के लिए, धारा 232 : संदर्भ (Reference) के लिए, धारा 233 : प्रकरणों के स्थानांतरण के लिए, धारा 258 : नियम बनाने के लिए।
राजस्व मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 375 तथा राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 5(35) के अंतर्गत एक न्यायालय है, जिसे अपने आदेशों के उल्लंघन पर अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं।
1. धारा 9 – अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का सामान्य पर्यवेक्षण: मंडल सभी राजस्व न्यायालयों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है तथा ऐसे सभी न्यायालय एवं अधिकारी इसके अधीनस्थ होते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 221 में भी है, जिसके अंतर्गत सभी राजस्व न्यायालयों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण मंडल में निहित होता है तथा सभी न्यायालय मंडल के अधीनस्थ रहते हैं।
2. धारा 10 – मंडल का अधिकार क्षेत्र किस प्रकार प्रयोग किया जाए: मंडल का अधिकार क्षेत्र अध्यक्ष अथवा मंडल का कोई अन्य सदस्य अकेले बैठकर या फिर दो या अधिक सदस्यों वाली पीठ द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दो तरीके हैं – (i) एकल पीठ द्वारा, अथवा (ii) द्वि-पीठ अथवा बहु-पीठ द्वारा। किन-किन प्रकार के प्रकरण एकल पीठ और द्वि/बहु-पीठ द्वारा सुने जाएंगे, यह राजस्थान राजस्व न्यायालय नियमावली में निर्धारित है।
नियम 8 – एकल पीठ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अंतर्गत द्वितीय अपीलें सुनता एवं निपटाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रकरणों के स्थानांतरण हेतु आवेदन, पुनरीक्ष, संदर्भ आदि की सुनवाई करता है।
नियम 9 – मंडल की द्वि-पीठ अपील के आधार पर मंडल के विचाराधीन आने वाले सभी डिक्री और आदेशों की सुनवाई और निपटारा करती है, सिवाय उन मामलों के जो नियम 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं। जब कोई मामला मंडल की पीठ द्वारा सुना जाता है, तो उस प्रकरण का निर्णय पीठ के सदस्यों की राय के अनुसार किया जाएगा।
विशेष अपील – यदि कोई पक्षकार किसी एकल सदस्य के निर्णय से आहत होता है, तो उसे उस निर्णय के खिलाफ दो या अधिक सदस्यों वाली पीठ के समक्ष विशेष अपील करने का अधिकार है, बशर्ते कि निर्णय देने वाला सदस्य स्वयं यह घोषित करे कि मामला अपील योग्य है। केवल वही सदस्य, जिसने निर्णय दिया है, विशेष अपील की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम है; अन्य कोई सदस्य यह अनुमति नहीं दे सकता, विशेष अपील एकल पीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध स्वीकार्य नहीं होती, विशेष अपील पुनरीक्षण अधिकारिता के अंतर्गत मंडल द्वारा पारित आदेशों पर भी लागू नहीं होती।
1. धारा 11 – मामले को पीठ को संदर्भित करने की शक्त: अध्यक्ष या कोई भी सदस्य, जो किसी प्रकरण या कार्यवाही का निपटारा अकेले कर रहा हो, यदि उचित समझे, तो कारण लिखित रूप से अभिलेखित करते हुए किसी भी विधि संबंधी प्रश्न अथवा प्रथा (जिसे विधि का बल प्राप्त हो) को पीठ के मतार्थ संदर्भित कर सकता है। तत्पश्चात प्रकरण का निपटारा उस मत के अनुसार किया जाएगा। न्यायिक दृष्टांत यह इंगित करता है कि इस धारा के अंतर्गत शक्तियों का विस्तार कर दिया गया है, जिससे द्वि-पीठ द्वारा किसी मामले को बड़ी पीठ या पूर्ण पीठ को संदर्भित करना भी सम्मिलित है।
2. धारा 12 – प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति :यदि किसी मामले में किसी पीठ को यह प्रतीत होता है कि धारा 11 में वर्णित कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय का मत प्राप्त करना आवश्यक है, तो पीठ उस प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकती है। उच्च न्यायालय, जैसा वह उचित समझे, सुनवाई के पश्चात् उस प्रश्न पर अपना मत अभिलेखित करेगा और मामले का निर्णय उसी मत के अनुरूप होगा।
3. धारा 13 – मतभेद की स्थिति में निर्णय : जब कोई मामला मंडल की किसी पीठ द्वारा सुना जाता है, तो उस प्रकरण का निर्णय उस पर सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत के मत के अनुसार किया जाएगा। यदि सदस्यों में इस बात को लेकर मतभेद हो कि मामले में क्या आदेश पारित किया जाए, तो प्रकरण को किसी अन्य सदस्य को संदर्भित किया जाएगा और उस सदस्य सहित बहुमत के मत के अनुसार निर्णय पारित किया जाएगा।
4. धारा 14 – मंडल की अभिलेख-पुस्तकें (Registers) : मंडल अपने कार्यों के निष्पादन हेतु, नियमों द्वारा या आवश्यकता अनुसार, ऐसी अभिलेख-पुस्तकें एवं लेखा-पुस्तकें रखेगा और उनका संधारण करेगा। मंडल द्वारा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिन अभिलेख-पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है, उनकी सूची इस धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है।
राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955
राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की महत्वपूर्ण धाराएँ इस प्रकार हैं:
• खातेदारी अधिकारों का प्रदत्तिकरण: धाराएँ 13, 15 और 19
• विक्रय, उपहार एवं वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध: धारा 42
• विशेष परिस्थितियों में भू-धारण का किराये पर देना या उप-किराये पर देना (देवस्थल भूमि के मामले में): धारा 46
• भू-धारण का बंटवारा: धारा 53
• घोषणात्मक वाद: धारा 88
• अवैध हस्तांतरण के लिए बेदखली: धारा 175
• ग़लत तरीके से बेदखली के विरुद्ध निषेधाज्ञा: धारा 188
• निषेधाज्ञा और रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान: धारा 212
• न्यायालय कार्य में महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत
अस्थायी निषेधाज्ञाओं का निर्णय करते समय राजस्व न्यायालयों को उन सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है जिनके आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है, अर्थात् –(a) वादी के पास एक प्रथमदृष्टया मामला होना चाहिए। (b) न्यायालय का हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक हो कि वादी को, अपने विधिक अधिकार का परीक्षण द्वारा सिद्ध होने से पहले, अपरिवर्तनीय क्षति से बचाया जा सके। (c) सुविधा का संतुलन अर्थात निषेधाज्ञा दिए जाने या न दिए जाने से किस पक्ष को अधिक सुविधा या असुविधा होगी। सामान्यतः किसी दर्ज खातेदार किरायेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, राजस्थान किरायेदारी अधिनियम के अंतर्गत देवता की स्थिति एक महत्वपूर्ण विधिक व्याख्या का विषय है। अनेक मामलों में, जो राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत हैं, देवता के नाम दर्ज भूमि पर खातेदारी अधिकार का दावा किया गया है। यह आवश्यक है कि राजस्व न्यायालय देवता की भूमि से संबंधित विधिक प्रावधानों से पूरी तरह अवगत हों, कई बार ऐसा हुआ है कि देवता की भूमि पूजारी के नाम दर्ज हो गई और उसके बाद तीसरे पक्ष को हस्तांतरण कर दिया गया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देवता को सदैव अल्पवयस्क माना जाता है। अतः जहाँ-जहाँ इस प्रकार के म्यूटेशन या अधिकार अभिलेख प्रविष्टियाँ मौजूद हों, वहाँ धारा 82 के अंतर्गत संदर्भ की कार्यवाही प्रारंभ करना अनिवार्य है, यह राजस्व न्यायालयों का कार्य नहीं है कि वे यह तय करें कि किसी विशेष देवता का पूजारी कौन है। यह अधिकार केवल नागरिक न्यायालयों का है।
न्याय वितरण प्रणाली में सुधार
लगातार सरकारें न्याय वितरण प्रणाली में सुधार की बात करती रही हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें गंभीर और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। राजस्व मंडल में द्वितीय अपीलों का निर्णय होने में 15 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। अधिकांश फौजदारी वाद राजस्व न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में अत्यधिक देरी से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वादी कानून अपने हाथ में लेने को विवश हो जाता है। यह अनवरत विलंब वादी के लिए अन्यायपूर्ण बन गया है।
न्याय प्रशासन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन 5 अप्रैल 2015 को बुलाया। उस समय भारत में 2.64 करोड़ मामले अधीनस्थ न्यायालयों में और 42 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित थे। सम्मेलन के एजेंडे में अवसंरचना विकास, न्यायिक सुधार, न्यायालयों का आईसीटी (ICT) सक्षम बनाना, लंबित मामलों को कम करने और शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ठोस कदम शामिल थे। न्याय वितरण प्रणाली का व्यापार सुगमता में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू किया गया, जिसके तहत हजारों न्यायालयों के मामले का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जिसमें अधिकांश उच्च न्यायालय शामिल हैं, को न्यायपालिका के लिए उपलब्ध कराया गया ताकि केस और कोर्ट प्रबंधन व न्यायिक कार्यकुशलता में सुधार हो सके। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में न्यायिक अकादमियों को सशक्त बनाना, लोक अदालतों को बढ़ावा देना और न्यायाधीशों का प्रशिक्षण शामिल थे।
भारत सरकार ने न्यायिक सुधारों को गति देने के लिए कानूनी सहायता और सशक्तिकरण की अनेक पहलें शुरू कीं। तीन प्रमुख पहलें थीं – प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ, टेली-लॉ सेवा न्याय मित्र योजना सरकार ने यह भी कहा कि देश की न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण किया जाएगा क्योंकि डिजिटल समावेशन ही डिजिटल इंडिया की दिशा में प्रगति की कुंजी है। प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ: यह एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इच्छुक वकील स्वयं को पंजीकृत कर गरीब एवं वंचित वादकारियों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। टेली-लॉ सेवा: इसका उद्देश्य था राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) में तैनात विशेषज्ञ वकीलों के पैनल के माध्यम से वादकारियों को कानूनी परामर्श उपलब्ध कराना। न्याय मित्र योजना: इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यपालक अधिकारी, जिनके पास विधिक अनुभव है, को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त कर कॉमन सर्विस सेंटरों पर तैनात किया गया। उनका कार्य था नेशनल जुडिशियल ग्रिड के माध्यम से लंबित मामलों की पहचान करना और त्वरित विवाद निपटान सुनिश्चित करना।
भारत सरकार ने ई-कोर्ट्स पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) को जिलों की वेबसाइटों और नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के माध्यम से लागू किया। यह पोर्टल वादकारियों को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है जैसे – केस पंजीकरण का विवरण, कारण सूची, केस की स्थिति, दैनिक आदेश, अंतिम निर्णय।
राजस्व मंडल में महत्त्वपूर्ण सुधार
राजस्थान का राजस्व मंडल राज्य स्तर की उन संस्थाओं में से एक था, जिसकी स्थापना राजस्थान के गठन के समय अजमेर में की गई थी। अन्य संस्थाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आयुर्वेद निदेशालय शामिल थे।यह संस्था 70 वर्षों की न्याय मंदिर जैसी विरासत लिए हुए थी। यह भारत के सबसे पुराने राजस्व मंडलों में से एक है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मंडल भी शामिल हैं, जिनकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। राजस्थान का राजस्व मंडल सदस्यों की संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा था और इसने सबसे अधिक राजस्व मामलों का निस्तारण किया।
राजस्व मंडल सभी प्रचलित अधिनियमों के अंतर्गत मुख्य नियंत्रणकारी राजस्व प्राधिकारी है। मुख्य नियंत्रणकारी राजस्व प्राधिकारी होने के नाते यह राज्य सरकार का एक अंग है और इसे विभिन्न अधिनियमों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। यह राजस्थान की सर्वोच्च राजस्व अपीलीय, पुनरीक्षण एवं संदर्भ न्यायालय है, जिसे अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर सर्वसाधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।वर्ष 1974 में राज्य सरकार ने गैर-न्यायिक प्रकृति के मामलों (जो सेटलमेंट से संबंधित नहीं थे) में अपनी पुनरीक्षणीय शक्तियाँ राजस्व मंडल को सौंप दी थीं। भूमि अभिलेखों का कार्य भी राजस्व मंडल को सौंपा गया है, जो प्रशासनिक प्रकृति का होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।
राजस्व मंडल एक ऐसी संस्था थी जो अत्यधिक मामलों के बोझ से ग्रस्त थी और तकनीकी दृष्टि से भी लगभग अप्रचलित हो चुकी थी, क्योंकि डिजिटलीकरण की व्यवस्था अस्तित्वहीन थी। हजारों फाइलों की स्थिति की मैनुअल निगरानी करना असंभव था। प्रतिदिन लगभग 5000 वादी और 1000 अधिवक्ता राजस्व मंडल की 14 कार्यरत पीठों में उपस्थित होते थे। बहुत ही कम मामलों में बहसें सुनी जाती थीं और निपटान का औसत मात्र 450 मामले प्रतिमाह था। संस्था को तत्काल मौलिक सुधारों और रूपांतरणकारी शासन की आवश्यकता थी। मेरी 18 माह की अध्यक्षीय अवधि के अंत तक, मामलों के निपटान का औसत प्रति माह दोगुना हो गया। अच्छे शासन की मुख्य आधारशिलाएँ थीं—अध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन पीठ का संचालन, समय पर बहसों और समय पर निर्णयों पर ध्यान, तथा राजस्व मंडल का डिजिटलीकरण।
राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में, मुझे राजस्थान की राजस्व न्यायालयों का डिजिटलीकरण करने, निरीक्षणों को सुदृढ़ कर प्रणालीगत दक्षता बढ़ाने, न्यायालयों की बैठकों की भविष्यवाणी और स्थिरता में सुधार करने तथा राज्यभर में हजारों अधिवक्ताओं से संवाद कर उन्हें तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर, पीठ और बार के बीच संबंध सुधारने का अवसर मिला। मेरे कार्यकाल में राजस्व मंडल में संस्थागत निर्माण चार स्तंभों पर आधारित था - न्यायशास्त्र संबंधी मुद्दों की गहन पड़ताल, निर्णय लेने की गति को तेज करना, तकनीक के प्रभाव को गहरा करना, क्षमता निर्माण की पहल को मजबूत करना तथा प्रशासनिक/न्यायिक प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करना।
राजस्थान में सम्मिलित किए गए राजपुताना के राज्यों में किरायेदारी की विभिन्न प्रथाएँ प्रचलित थीं। राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के बाद जब भूमि-जोतने वाले को भूमि की नीति को लागू किया गया, तब किरायेदारी और भू-सीमा निर्धारण मामलों में भारी मात्रा में वाद-विवाद बढ़ गए। राजस्थान की राजस्व न्यायालयों में 5.74 लाख मामले लंबित थे जिनका निस्तारण किया जाना था। किरायेदारी प्रथाओं को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत सिद्धांत थे-सामुदायिक भूमि की सुरक्षा, कन्या संतानों के अधिकारों की रक्षा, कृषक प्रधान जिलों में “बल ही अधिकार है” जैसी प्रवृत्तियों को रोकना, मंदिर की भूमि की सुरक्षा, तथा जोतों के विभाजन को तहसीलदार की देखरेख में करना।
मामलों के त्वरित निस्तारण
राजस्व मंडल में न्यायालयीय कार्य में सुधार लाने के दो प्रमुख तरीके थे: (a) आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सदस्यों द्वारा उच्चतर निस्तारण प्राप्त करना, तथा (b) अधिवक्ताओं का पीठ के साथ सहयोग करना ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। पूर्ण मामले, जिन्हें पीठ के पास भेजा जाता था, और अपूर्ण मामले, जिनका निस्तारण रजिस्ट्री स्तर पर किया जाता था।इन मामलों को मासिक आधार पर अपडेट किया जाता था जिससे रजिस्ट्री के कार्य की स्पष्ट जानकारी मिलती थी। रजिस्ट्री इस बात के लिए उत्तरदायी थी कि प्रवेश एवं प्रलेखन की प्रारंभिक प्रक्रियाएँ तथा समन की सेवा समय पर पूरी की जाएँ। राजस्थान राजस्व बार के साथ नियमित विचार-विमर्श से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। न केवल बार की हड़तालें पूरी तरह समाप्त हुईं बल्कि सकारात्मक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। रजिस्ट्री द्वारा पीठ को तर्क-वितर्क के लिए भेजे जाने वाले पूर्ण मामलों की संख्या आठ प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 प्रतिदिन कर दी गई। समन की सेवा अभियान चलाए जाने से रजिस्ट्री में पूर्ण मामलों की कुल संख्या बढ़कर 22,000 तक पहुँच गई।
राजस्व न्यायालयों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव – एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर
राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में पहली डिजिटल क्रांति के लिए विभिन्न हितधारक एक साथ आए। ट्रायल कोर्ट से लेकर राजस्व मंडल तक न्यायालयों के फैसलों और डिक्री तक सार्वभौमिक पहुँच उपलब्ध कराने का निर्णय, राजस्व न्यायालयों में प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ‘ई-मित्र प्लस’ पर (RCMS) उपलब्ध कराने का अर्थ था कि अब राजस्थान के 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में न्यायालय के निर्णय डाउनलोड किए जा सकते थे। न केवल हर राजस्व न्यायालय के निर्णय तकनीकी मंच पर उपलब्ध हुए, बल्कि राजस्व न्यायालयों में लंबित 5,70,000 मामलों की स्थिति भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही अनेक सुविधाएँ प्रारंभ की गईं-नए दाख़िल मामलों में अधिवक्ताओं के लिए SMS सुविधा, निर्णयों पर ई-सिग्नेचर, RCMS मोबाइल ऐप, राजस्व न्यायालयों के कार्य की ऑनलाइन निगरानी। RCMS प्लेटफ़ॉर्म ने प्रत्येक राजस्व न्यायालय के कार्यों का समग्र आकलन उपलब्ध कराया कितनी बैठकें हुईं, कितने मामले सुने गए और कितने निर्णय एवं डिक्री सुनाई गईं।राजस्व मंडल में सदस्यों को प्रतिदिन निर्णयों एवं डिक्री की स्थिति की जानकारी दी जाती थी